NEWS & POLITICSसमाचार और राजनीति
BAHUJAN CULTUREबहुजन संस्कृति
बेड़ियाँ तोडती स्त्री : लता सिंह
लेखक अरविंद जैन बता रहे हैं लता सिंह की कहानी। लता सिंह ने अंतर जातीय विवाह किया। उनके नाराज भाईयों ने उनके पति व उनके परिजनों पर न सिर्फ बेइंतहां जुल्म ढाये बल्कि उन्हें मुकदमों के पेंच में फंसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। बावजूद इसके भारतीय कानून में अब भी कई खामियां मौजूद हैं
BY ARVIND JAIN अरविंद जैन ON JULY 13, 2019 NO COMMENTSREAD THIS ARTICLE IN ENGLISH
न्याय क्षेत्रे-अन्याय क्षेत्रे
(राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2014 में 28 ऑनर किलिंग के मामले दर्ज किए गए, 2015 में 251 और वर्ष 2016 में 77। मतलब यह कि 2014 से 2016 के बीच तीन सालों में ही ‘ऑनर किलिंग’ के 356 मामले दर्ज किए गए। अधिकांश मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं।)
अंतर्जातीय विवाह और ‘ऑनर किलिंग’
लता सिंह से लेकर बबली और अन्य जाति-धर्म की बेड़ियाँ तोड़ने वाले रोशन दिमाग युवा समाज की नायिका है, मगर परम्परावादी परिवारों में ‘खलनायिका’। लता सिंह लड़-लड़ कर जिंदा है और बबली की हत्या हो चुकी है। किसी भी हत्यारे को अभी तक फाँसी नहीं हुई…जिन्हें हुई वो उम्र कैद बदल (दी) गई।

उन्नीस साल पहले एक युवा लड़की थी लता सिंह। उम्र 27 साल, युवा महिला जो स्नातक की पढाई कर चुकी थी और प्रासंगिक समय पर लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी में परास्नातक पाठ्यक्रम कर रही थी। माता-पिता की अचानक मृत्यु के बाद वह अपने भाई अजय प्रताप सिंह के साथ एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ में रहने लगी, जहाँ उसने 1997 में इंटरमीडिएट किया और 2000 में स्नातक की पढ़ाई की। उसी साल 2 नवम्बर को उसने अपनी मर्जी से अपने भाई का घर छोड़ दिया और दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में ब्रम्हा नंद गुप्ता से शादी कर ली। पति का दिल्ली और अन्य जगहों पर कारोबार था (और विवाह के बाद उनका एक बच्चा भी।) दो दिन बाद ही लता सिंह के भाई ने सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन, लखनऊ में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और इसके परिणामस्वरूप पुलिस ने लता सिंह के पति की दो बहनों और उसके पति के चचेरे भाई के साथ दो बहनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में ममता गुप्ता, संगीता गुप्ता (ब्रह्म नंद गुप्ता की बहनें), साथ ही राकेश गुप्ता (ममता गुप्ता के पति) और लता सिंह के पति कल्लू गुप्ता चचेरे भाई थे। ममता अपने एक महीने के बच्चे के साथ जेल में थी।

सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली
लता सिंह के भाई अजय प्रताप सिंह, शशि प्रताप सिंह और आनंद प्रताप सिंह उग्र थे, क्योंकि उसने अंतर-जातीय विवाह किया था, और इसलिए वे उसके पति के पैतृक निवास गए और उसके पति की माँ और चाचा की जमकर पिटाई की। घर से सामान, फर्नीचर, बर्तन आदि फेंक दिया और अपने ताले से बंद कर दिया। उसके पति के एक भाई को कथित रूप से भोजन और पानी के बिना चार-पांच दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके पति के कृषि क्षेत्र की फसल की फसल काट ली और उसे बेच दिया, और उन्होंने खेत पर जबरन कब्जा भी कर लिया। उन्होंने पुलिस थाने सरोजनी नगर, लखनऊ में अपने पति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ अपहरण का आरोप लगाते हुए एक झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, जिसके कारण उसके पति और एक बहन के पति को गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में लिया गया जो लखनऊ जेल में हैं। उसके भाइयों ने अवैध रूप से उसके पति की दुकान को भी अपने कब्जे में ले लिया।
उसके पति और उसके रिश्तेदारों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और अपहरण कर उसे भी मार सकते थे। गुप्ता परिवार के सदस्य भाइयों द्वारा हिंसा के डर से लखनऊ जाने से डरते थे, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उसके पति के तीन रिश्तेदारों को लंबे समय तक जमानत नहीं दी गई और उनका जीवन बर्बाद हो गया, हालांकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था। अपने पति और रिश्तेदारों को उत्पीड़न से बचाने के लिए उसने राजस्थान महिला आयोग, जयपुर से संपर्क किया। आयोग ने 13 मार्च, 2001 को उसका बयान दर्ज किया और आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक (शहर), लखनऊ को भेज दिया। आयोग की अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखकर आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बाद में सूचित किया कि सभी आरोपी व्यक्तियों को 17 मई, 2001 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इसके बाद (28 मई, 2001) जांच अधिकारी ने लता गुप्ता उर्फ़ लता सिंह का बयान दर्ज किया और सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की गई। अगले दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने भी धारा 164[1] के तहत उसका बयान दर्ज किया। बयान में लता ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से ब्रम्हा नंद गुप्ता से शादी की। इस कथन के बावजूद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए (कि पुलिस ने पहले ही मामले में अंतिम रिपोर्ट दे चुकी है) मुकदमा आगे चलने का आदेश (5 अक्टूबर, 2001) जारी कर दिया। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि लता सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। हालांकि, उसकी मानसिक रूप से मनोरोग केंद्र, जयपुर के बोर्ड द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट, लखनऊ (जिसके समक्ष सभी चार आरोपियों के खिलाफ मामला लंबित था) ने गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के खिलाफ, आरोपी ने धारा 482[2] आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) में एक याचिका (नंबर 520/2003) दायर की।। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को सत्र न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जो स्वयं यह जांच करेगा कि आरोपी ने कोई अपराध किया है या नहीं। मामला अभी भी लंबित है।
यह भी पढ़ें : बेड़ियां तोड़ती स्त्री : करुणा प्रीति
लता को समझ ही नहीं आया कि कानून तो ऐसे ही अपना काम करता (रहता) है! यह सब झेलने के बाद लता सिंह ने (वरिष्ठ वकीलों की ‘कानूनी सलाह’ पर) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करना और सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही बेहतर समझा। उसने अपनी याचिका में उपरोक्त तथ्यों का हवाला देते कहा कि वह लखनऊ नहीं जा सकती, क्योंकि उसके अपने, अपने पति और छोटे बच्चे के जीवन के लिए खतरा है। उसने आगे आरोप लगाया है कि उसके भाइयों ने उसके पति ब्रम्हा नंद गुप्ता के पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, अपमानित किया और अप्रासंगिक रूप से नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि दूरदराज के रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मकान और कृषि भूमि और दुकानों सहित उनकी संपत्तियों को उसके भाइयों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था और उसके और उसके पति की जान को लगातार खतरा है क्योंकि उनके भाई उन्हें धमकी दे रहे हैं।
तमाम तथ्यों का गंभीरतापूर्वक विवेचन के बाद न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और अशोक भान ने कहा “इस केस से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता बालिग़ है और सभी प्रासंगिक समय में बालिग़ थी। इसलिए वह किसी से भी शादी करने या साथ रहने के लिए स्वतंत्र है, जिसे वह पसंद करती है। हिंदू विवाह अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत अंतर-जातीय विवाह पर कोई रोक नहीं है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि याचिकाकर्ता, उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों ने कोई अपराध किया है।
हमारा विचार है कि किसी भी आरोपी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया और विचाराधीन पूरा आपराधिक मामला अदालत की प्रक्रिया के साथ-साथ याचिकाकर्ता के भाइयों के प्रभाव में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग है, जो केवल इसलिए उग्र थे क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपनी जाति के बाहर शादी की। हम यह सुन कर व्यथित हैं कि याचिकाकर्ता के भाइयों के खिलाफ उनके गैरकानूनी कार्यों (जिसका विवरण ऊपर सेट किया गया है) के लिए कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही की है।
चूंकि ऐसे उत्पीड़न, खतरों और युवक और युवतियों के खिलाफ हिंसा के बारे में पता चल रहे हैं, जो अपनी जाति से बाहर शादी करते हैं, इसलिए हम इस मामले पर कुछ सामान्य टिप्पणी करना आवश्यक समझते हैं। राष्ट्र हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन अवधि (जैसे कि वर्तमान) से गुजर रहा है, और यह न्यायालय महान सार्वजनिक चिंता के मामलों में चुप नहीं रह सकता है।”[3]
जाति व्यवस्था राष्ट्र के लिए एक अभिशाप
न्यायमूर्तियों ने अपने निर्णय में उल्लेख किया “जाति व्यवस्था राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है और जितनी जल्दी इसे नष्ट किया जाए उतना ही बेहतर है। वास्तव में, यह राष्ट्र को ऐसे समय में विभाजित कर रहा है, जब हमें एकजुट होकर राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों का सामना करना होगा। इसलिए, अंतर-जातीय विवाह वास्तव में राष्ट्रीय हित में हैं क्योंकि इससे जाति व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। हालांकि, देश के कई हिस्सों से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि जो युवक और युवतियां अंतरजातीय विवाह से गुजरते हैं, उन्हें हिंसा की धमकी दी जाती है, या उन पर वास्तव में हिंसा की जाती है। हमारी राय में, हिंसा या धमकी या उत्पीड़न के ऐसे कार्य पूरी तरह से अवैध हैं और उन्हें करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार एक व्यक्ति बालिग़ हो जाता है या वह जिसे भी पसंद करता है उससे शादी कर सकता है। यदि लड़का या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंधों को काट सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं। कोई उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता है जो इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरता है। इसलिए, हम यह निर्देश देते हैं कि देश भर में प्रशासन / पुलिस अधिकारी यह देखेंगे कि यदि कोई भी लड़का या लड़की एक बालिग़ महिला के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है या एक बालिग़ पुरुष है, युगल हैं किसी को भी परेशान नहीं किया जाए और न ही हिंसा के खतरों या कृत्यों के अधीन, और कोई भी जो ऐसी धमकियां देता है या उत्पीड़न करता है या हिंसा का कार्य करता है या खुद अपने दायित्व पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का काम लिया जाता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, जो कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं। हम कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों के `सम्मान’ हत्या के बारे में सुनते हैं, जो अपनी मर्जी से अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरते हैं। इस तरह की हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है, और वास्तव में वे क्रूर, सामंती दिमाग वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए हत्या के बर्बर और शर्मनाक कृत्य के अलावा कुछ नहीं हैं, जो कठोर सजा के पात्र हैं। केवल इस तरह से हम बर्बरता के ऐसे कृत्यों को समाप्त कर सकते हैं।“
माननीय न्यायमूर्तियों ने उपरोक्त परिस्थितियों में याचिका स्वीकार करते हुए मुकदमा और आरोपियों के खिलाफ वारंट भी रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि सभी संबंधित स्थानों की पुलिस को यह सुनिश्चित करना है कि याचिकाकर्ता, उसके पति और न ही किसी रिश्तेदार को परेशान किया जाए या धमकी दी जाए और न ही उनके खिलाफ हिंसा का कोई कार्य किया जाए। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उसे संबंधित अधिकारियों द्वारा, कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस तरह लता सिंह ने अपने (और अपने परिवार) वैधानिक अधिकारों की रक्षा और अंतर्जातीय विवाह करने की स्वतंत्रता के लिए, जो कानूनी लड़ाई लड़ी वो आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का पाठ भी है और महतवपूर्ण नजीर भी। निसंदेह भारत में सगोत्र विवाह कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं। इस संबंध में किसी भी तरह की (हर) शंका को दूर करने के लिए, कानून[4]पारित किया गया था। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि एक ही गोत्र या ‘प्रवर’ या एक ही जाति के विभिन्न उप-डिवीजनों से संबंधित हिंदुओं के बीच विवाह वैध माने-समझे जायेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम[5] में भी सगोत्र या अंतरजातीय विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियों की पीठ (दीपक मिश्र, ए.एम. खानविलकर और धनंजय चंद्रचूड) ने 27 मार्च, 2018 को एक महत्वपूर्ण मामले[6] में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसके अनुसार सम्मान आधारित हिंसा को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस फैसले में खाप पंचायत को गैर-कानूनी घोषित किया गया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दो वयस्क अगर शादी करते हैं तो कोई तीसरा उसमें दखल नहीं दे सकता है। इसके अलावा न्यायालय ने हिन्दू विवाह अधिनियम की (धारा 5) में एक ही गोत्र में शादी करने को उचित ठहराया है।
यही तो है धर्मनिरपेक्षता!
मगर दुर्भाग्य से, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में विशेष विवाह कानून[7] के तहत अंतर्जातीय विवाह को संचालित करने वाले बुनियादी कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस कानून के तहत शादी के अंजाम संबंधी चौथे अध्याय में अंतर्जातीय विवाह को हतोत्साहित करते हैं। धारा-19 के मुताबिक, इस कानून के तहत शादी किसी अविभक्त हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन अन्य धर्मावलंबी परिवार में आयोजित होती है, तो ऐसे परिवार से उन्हें अलग कर दिया जाएगा। कानून ऐसे हिंदू बौद्ध, सिख या जैन को आजादी देता है, जो अविभक्त परिवार के सदस्य हैं। ऐसे लोग अन्य धर्मो में शादी करते हैं तो शादी के दिन से उनके अपने परिवार के साथ रिश्ते अपने आप टूट जाएंगे। यह परोक्ष रूप से अवरोध निर्मित करता है और ऐलान करता है कि हम आपको गैर हिंदू पत्नी या पति को अपने परिवार में कबूल नहीं करेंगे। आप अपने अविभक्त परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा, यदि कोई हो, लेते हैं तो परिवार से भी हाथ धोना पड़ेगा। विशेष कानून भी मानता है कि हिन्दू परिवार में विधर्मी बहू या दामाद का क्या काम!
सुप्रीम कोर्ट ने (लता सिंह केस) भी इस बात को रेखांकित किया है कि अगर लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसी अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक शादी को मंजूरी नहीं देते, तो वे अपने पुत्र या पुत्री से सामाजिक रिश्ते तोड़ सकते हैं। कोर्ट ने ठीक ही आगाह किया है कि ऐसी शादियां कर चुके लोगों को घर वाले किसी तरह की न तो धमकी दे सकते हैं और न ही मारपीट कर सकते हैं। वे इन्हें यातना भी नहीं दे सकते।
बदलते समय में सामाजिक न्याय के बीज
जाति व्यवस्था वाले ऐसे पारंपरिक समाज में, शादी के लिए चुनाव काफी अहम हो जाता है। ऐसे में, अपनी जाति या धर्म से हटकर शादी के बारे में सोच पाना आसान नहीं। हालांकि, भारत में शादी के तरीके में आया हाल का बदलाव अंतर्जातीय शादियों, खासकर आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के चलते बढ़त दर्शा रहा है। पंजाब, हरियाणा, असम और महाराष्ट्र में फिर भी अंतर्धार्मिक शादियों को अब भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में पारंपरिक और सामंती मानसिकता में बदलाव काफी कम देखा गया है। इसलिए हमें निर्दोष युवा लड़के और लड़कियों को ‘ऑनर किलिंग’ से बचाने के लिए एकजुट होने की अधिक जरूरत है। ये वे युवा हैं, जो जाति और वर्ग रहित समाज में जीने की कामना रखते हैं। अगर न्यायिक व्याख्याएं लैंगिक न्याय को स्वीकार नहीं करतीं, तो बदलते समय में सामाजिक न्याय के बीज कैसे अंकुरित होंगे?
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मार्कडेय काटजू और न्यायमूर्ति अशोक भान ने (लता सिंह केस) में व्यवस्था दी कि अंतर्जातीय विवाह से ही जाति नष्ट होगी दूसरी ओर, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था भारतीयों के दिमाग में रचा-बसा है। किसी कानूनी प्रावधान के न होने की सूरत में अंतर्जातीय शादियों होने पर कोई भी व्यक्ति अपने पिता की जाति का सहारा विरासत में लेता है, न कि मां का।[8] सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एच. के. सीमा और डॉ. ए आर लक्ष्मणन ने अर्जन कुमार मामले में स्पष्ट कहा कि ‘यह मामला आदिवासी महिला की एक गैर आदिवासी पति से शादी करने का है। पति कायस्थ है, इसलिए वह अनुसूचित जनजाति के होने का दावा नहीं कर सकता।’[9] एक भारतीय बच्चे को जाति उसके पिता से विरासत में मिलती है, न कि मां से। अगर वह बिन ब्याही है और बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती, तो वह क्या करे? महिला अपने पिता की जाति से होगी और शादी के बाद पति की जाति की। आपकी जाति और धर्म, आपके पिता के धर्म/ जाति से जुड़ी होती है। कोई अपना धर्म बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं।
लता सिंह केस के कुछ साल बाद अरुमुगम सर्वई बनाम तमिलनाडु राज्य[10] में, न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्र ने लता सिंह के मामले में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए आगे कहा “हमने हाल के वर्षों में “खाप पंचायतों” (तमिलनाडु में “कट्टा पंचायत” के रूप में जाना जाता है) के बारे में सुना है, जो अक्सर विभिन्न जातियों और धर्मों के लड़कों और लड़कियों को जो विवाह करना चाहते हैं या विवाहित हैं, पर संस्थागत तरीके से ऑनर किलिंग या अन्य अत्याचार करने या उसे प्रोत्साहित करते हैं, या लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अलावा, जो कानून को अपने हाथों में लेते हैं, वो कंगारू अदालतें हैं,जो पूरी तरह से अवैध हैं।“
शिक्षा, संस्कार और जातीय ‘सम्मान’ की अवधारणा
विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य[11] मामले में जहां बहन द्वारा (विवाह के लिए) चुने गए युवक की हत्या उसके ही भाई द्वारा की गई थी। भाई जिसने अच्छे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की थी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और सी नाग्पप्प्न ने सज़ा के सवाल पर विचार करते समय पाया कि आरोपी व्यक्तियों ने सदियों से अपूरणीय भावनाओं और दृष्टिकोण को त्यागने की क्षमता हासिल नहीं कर पाए। शायद, उनकि इस परिकल्पना ने परेशान किया था कि यह वही विचार है जो इस समय में अनादिकाल से यहाँ पहुंचे हैं और अनंत काल तक बने रहना चाहते थे। आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने कहा: –
“कोई भी यह महसूस कर सकता है कि ‘मेरा सम्मान ही मेरा जीवन है’ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे की कीमत पर एक का सम्मान बनाए रखा जाए। स्त्री की स्वतंत्रता, आज़ादी, संवैधानिक पहचान, व्यक्तिगत पसंद और विचार, वो एक पत्नी हो या बहन या बेटी या मां, निश्चित रूप से शारीरिक बल या धमकी या अपने स्वयं के नाम पर मानसिक क्रूरता से नहीं रोका जा सकता है। इसके अलावा, न तो परिवार के सदस्यों और न ही सामूहिक सदस्यों को लड़की द्वारा चुने गए लड़के पर हमला करने का कोई अधिकार है। उसकी व्यक्तिगत पसंद उसका स्वाभिमान है और उसमें सेंध लगाना उसके सम्मान को नष्ट करना है। और उसकी अपनी पसंद को खत्म करके तथाकथित भाईचारे या पितृ सम्मान या वर्ग सम्मान को थोपना अति क्रूरता का अपराध है। इससे भी अधिक जब यह एक (सम्मान) आड़ में किया जाता है। यह “सम्मान” की एक निंदनीय धारणा है, जो मध्ययुगीन जुनूनी दावे के बराबर है।”
आशा रंजन बनाम बिहार राज्य[12] में और अन्य, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग संदर्भ में लिखा “जीवन में महिला को अपनी पसंद का साथी चुनने का वैध संवैधानिक अधिकार है। यह व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है जिसे अनुच्छेद 19 के तहत संविधान में मान्यता प्राप्त है, और इस तरह के अधिकार को “वर्ग सम्मान” या “समूह सोच” की अवधारणा से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं की सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामूहिक सम्मान की धारणा या भावना की कोई वैधता नहीं है, भले ही उसे सामूहिक रूप से लोग सही मानते हों।”
‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ न्यायिक विवेक
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण मास्टर और अन्य[13] में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी और जे. एम. पंचाल ने 3 अगस्त, 2010 को उच्च न्यायालय द्वारा बरी होने के फैसले को रद्द करते हुए आरोपी व्यक्तियों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने के साथ दोषी ठहराया। छह लोगों की हत्या और लगभग पूरे परिवार को मिटा देना और वह भी किसी सम्मान की फ़िल्मी कल्पना से इस अदालत द्वारा विकसित ‘दुर्लभतम’ मामले में आएगी इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सज़ा उचित है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना बीस साल से पहले हुई थी, उसने मौत की सजा नहीं पारित की लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उक्त निर्णय “सम्मान हत्या” के कारण होने वाले अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।“
अदालतें कहती रही (हैं) कि गांव के बुजुर्गों या परिवार के बुजुर्गों के विचारों को मानने के लिए, दंपति को मजबूर नहीं किया जा सकता है और किसी को भी बल का उपयोग करने या सामुदायिक सम्मान या पारिवारिक सम्मान के नाम पर दूरगामी प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि गलत कारावास, लगातार उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, गंभीर शारीरिक हानि या धमकी सहित कठोर कार्रवाई या तो निकट संबंध या कुछ तीसरे पक्षों द्वारा तथाकथित गलत जोड़े के खिलाफ या तो कुछ या सभी के उद्बोधन का सहारा लिया जाता है। पंचायतदारों या उनकी मिलीभगत से। एक या दूसरे जोड़े की हत्या के बहुत से उदाहरण खबरों में रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार और युवा जोड़े को प्रभावित करने वाले अन्य अवैध प्रतिबंधों में परिवारों और यहां तक कि स्थानीय निवासियों का एक वर्ग अक्सर इसका सहारा लेता है। यह सब परंपरा और सम्मान के नाम पर किया जाता है। ऐसे सभी अवैध कृत्यों का प्रभाव मूलतः सार्वजनिक व्यवस्था के आयाम भी हैं। दरअसल यही सब अन्तर्विरोध हैं, जो कानून और सामजिक मानसिकता के बीच बार-बार अवरोधक बन आ खड़े होते हैं। युवा स्त्रियों, युवकों. युगलों की बर्बर हत्या कि अनेक खौफनाक कहानियाँ हमारे आसपास बिखरी हैं और राष्ट्रीय अपराध के आंकड़े हमारे सामने है!
अंत में सिर्फ एक स्थाई स्मृति कि हरियाणा राज्य के जिला कैथल के करोरा गाँव के दो युवा (मनोज और बबली) एक ही गोत्र के थे। उनका कसूर था प्रेम करना और अपराध एक ही गांव-गोत्र के होते हुए विवाह करना। जून 2007 में बबली के रिश्तेदारों ने खाप पंचायत के आदेश पर उनकी हत्या कर दी थी। मार्च 2010 में करनाल की जिला अदालत ने तो बबली के परिवार के पांच सदस्यों- उसके भाई सुरेश, चाचा राजेंदर और बरू राम और चचेरे भाई सतीश और गुरदेव को मौत की सजा सुनाई थी, मगर मार्च 2011 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीशों ने मनोज-बबली सम्मान हत्या मामले में चार दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद की सजा में बदल दिया। अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन के चालक मनदीप सिंह को अपहरण और साजिश के लिए सात साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद मनोज की मां चंद्रपती, कानून के राज और न्याय व्यवस्था में कैसे विश्वास करे! तबाही के बाद उसकी चिता और तनाव कैसे कम होगा! क्या यही रास्ता है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और कुछ साल और इंसाफ का इंतज़ार! दो मासूम युवाओं को निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया मगर अपराध ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ नहीं (माना-समझा जाता) है। क्या खाप पंचायतें और बहुमत (हिन्दू समाज) कानून से ऊपर हैं? अगर न्याय के प्रहरियों और कानून के बीच टकराहट होती रहेगी, तो जाति और धर्म की बेड़ियों में जकड़ी स्त्री-पुरुष आजाद कैसे हो पायेगे? अराजक निजी कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं में आमूल-चूल बदलावों के बिना, अंतर्जातीय/अंतर्धार्मिक शादियों से जुड़े सामाजिक-आर्थिक राजनीति का मनोविज्ञान तेजी से नहीं बदल रहा…नहीं बदल सकता। कहां हैं सर्वोच्च न्यायालय के संविधानिक अधिकारों पर लिखे आदर्श वाक्य या सर्वश्रेष्ठ प्रवचन?
(कॉपी संपादन : नवल)
संदर्भ:-
[1] आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता,1973
[2] आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता,1973
[3] लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006 (5) एससीसी 475)
[4] हिंदू विवाह अक्षमता निवारण अधिनियम,1946
[5] हिंदू विवाह अधिनियम,1955
[6] शक्तिवाहिनी बनाम भारत संघ, 2018 (7) एससीसी 192
[7] विशेष विवाह कानून[7],1954
[8] 2003 एआईआर सुप्रीम कोर्ट, 5149
[9] 2006 एआईआर सुप्रीम कोर्ट, 1177
[10] 2011 (6) एससीसी 405
[11] 2016 (9) एससीसी 541
[12] 2017) 4 एससीसी 397
[13] 2010 (12) एससीसी 324
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
बहुजन साहित्य की प्रस्तावना
दलित पैंथर्स : एन ऑथरेटिव हिस्ट्री : लेखक : जेवी पवार
महिषासुर एक जननायक’
महिषासुर : मिथक व परंपराए
जाति के प्रश्न पर कबीर
चिंतन के जन सरोकार
शेयर
Click to share on Facebook (Opens in new window)
Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
Click to share on Twitter (Opens in new window)
Click to share on Pocket (Opens in new window)
Click to email this to a friend (Opens in new window)
Click to print (Opens in new window)
ABOUT THE AUTHOR

अरविंद जैन (जन्म- 7 दिसंबर 1953) सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। भारतीय समाज और कानून में स्त्री की स्थिति संबंधित लेखन के लिए जाने-जाते हैं। ‘औरत होने की सज़ा’, ‘उत्तराधिकार बनाम पुत्राधिकार’, ‘न्यायक्षेत्रे अन्यायक्षेत्रे’, ‘यौन हिंसा और न्याय की भाषा’ तथा ‘औरत : अस्तित्व और अस्मिता’ शीर्षक से महिलाओं की कानूनी स्थिति पर विचारपरक पुस्तकें। ‘लापता लड़की’ कहानी-संग्रह। बाल-अपराध न्याय अधिनियम के लिए भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य। हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए 'साहित्यकार सम्मान’; कथेतर साहित्य के लिए वर्ष 2001 का राष्ट्रीय शमशेर सम्मान
RELATED ARTICLES
बहुजन राजनीति का द्वंद्व और एकीकृत संघर्ष की चुनौतियाँ
ओबीसी के सामने दो रास्ते हैं। पहला, समाज के वंचित दलित-आदिवासी समूहों के साथ बेहतर सामंजस्य व समता का माहौल तैयार करते हुए भारत में व्यवस्था परिवर्त्तन में भूमिका निभाना। दूसरा, सामाजिक-राजनीतिक द्वंद्व के बीच दवाब के कारण मनुवादी-ब्राह्मणवादी समाज का पिछलग्गू बन तात्कालीक राजनीतिक-आर्थिक हित साधना
Dialectics of Bahujan politics and challenges to an integrated struggle
Two options are available to the OBCs. One, to join hands with the deprived Dalit-Tribals and become a co-partner in the intellectual and ideological battle for bringing about social justice and change in India. Two, to bow to the pressure from the Manuwadi-brahmanical community, follow in its footsteps and fulfil its political-economic agenda by patronizing status quoist and feudal values.
दलित उत्पीड़न क़ानून का अति पिछड़ी कामगार जातियों तक विस्तार की मांग
महाराष्ट्र के कोपर्डी में एक लड़की से बलात्कार के बाद महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के लोग सड़क पर हैं। उनकी कई मांगों में से एक मांग अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम को ख़त्म करना भी है, इस आशय का बयान मराठा क्षत्रप शरद पवार ने भी दिया है। हालांकि महाराष्ट्र ओबीसी संगठन इसे समाप्त करने की जगह इसके विस्तार की बात कर रहा है
‘Bring EBCs within the ambit of the Atrocities Act’
After the rape and murder of a girl in Kopardi, Maharashtra, the Maratha community of the state is up in arms. Among other things, it is demanding abrogation of the SC, ST (Prevention of Atrocities) Act. Maratha satrap Sharad Pawar has also backed the demand. The OBC organizations of Maharashtra, however, want that the ambit of the Act to be broadened.
सत्ता बदलते ही बिहार में दलितों पर अत्याचार बढ़ा
बीते 25 नवंबर को भागलपुर के नवगछिया इलाके के झंडापुर गांव में एक दलित के घर में घुसकर तीन लोगों की नृशंस हत्या कर दी गयी। जवान बेटी को अर्द्धनग्न कर तबतक पीटा गया जबतक कि वह बेहोश नहीं हो गयी। पुलिस के मुताबिक इस घटना का गवाह कोई नहीं है। लेकिन क्या यह केवल सामान्य अपराध की घटना है या बिहार में सत्ता के बदले समीकरण का असर, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार :
In Bihar, atrocities against Dalits have increased since regime change
On 25 November, three members of a Dalit family were murdered in their home in a village called Jhandapur, in the Naugachia area of Bhagalpur, Bihar. The young daughter was stripped half-naked and beaten unconscious. The police claim there are no witnesses to the incident. Is this incident representative of the crimes that have become common under the new coalition ruling Bihar? Nawal Kishore Kumar finds out
REPLY
भारत के पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और उनके सरोकारों को नए परिप्रेक्ष्य से देखने और गहराई से समझने का प्रयास है फॉरवर्ड प्रेस. चुप कर दिए गए बहुसंख्यक दलितबहुजनों की आवाज़ है फॉरवर्ड प्रेस. हमारे मिशन के बारे में अधिक जानें
एफपी साप्ताहिकी
फॉरवर्ड प्रेस साप्ताहिकी की सदस्यता लें और हर सप्ताह ताजे लेख ईमेल से पाएं। यह एकदम निःशुल्क है।
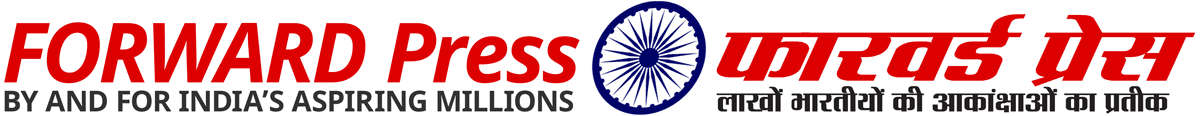




No comments:
Post a Comment